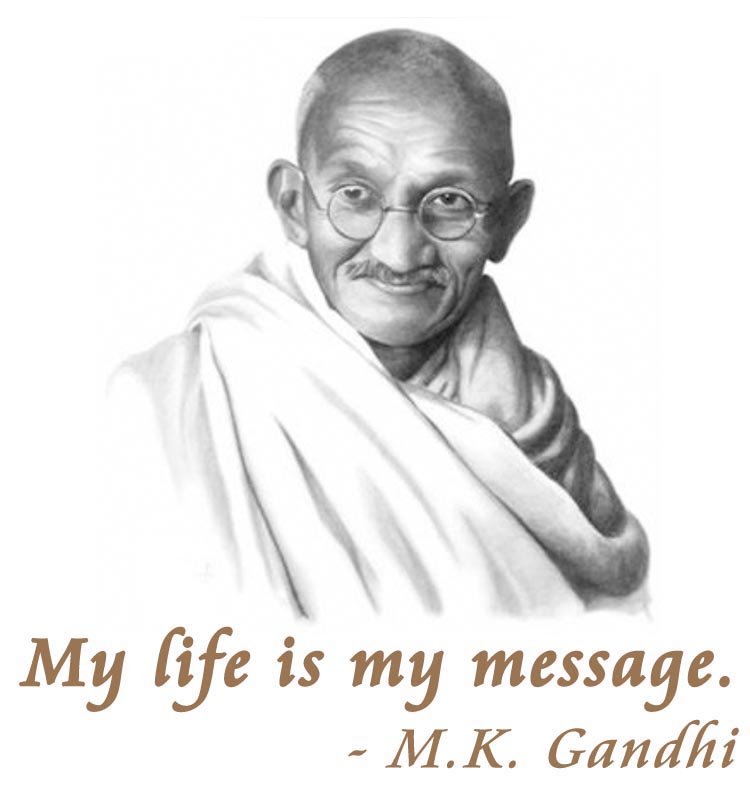
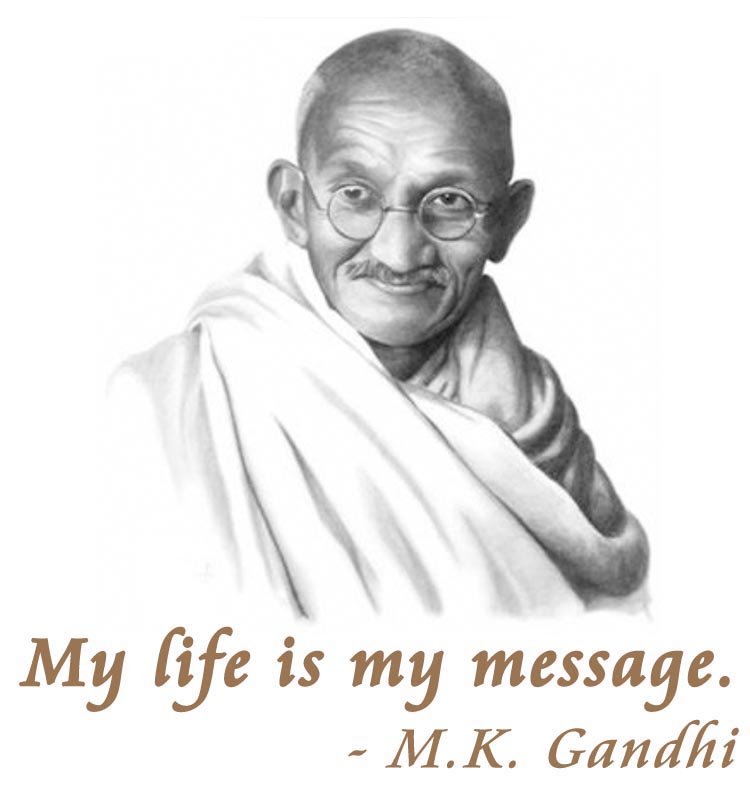
गांधी का राजनीतिक चेहरा |
- हिलाल अहमद भारतीय इतिहास के अत्यंत विस्फोटक दौर में महात्मा गांधी सबसे विस्फोटक हस्तक्षेप करते हैं और राजनीति की आधार-भूमि बदल देते हैं | वे राजनीति का मानवीय चेहरा उजागर ही नहीं करते हैं बल्कि उसका पूरा तंत्र व कार्यक्रम भी हमारे सामने रखते हैं | “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम!” शुरु करता हूं अल्लाह के नाम से ! इस तरह अपनी बात शुरु करने का मेरा मकसद न तो अपनी मुस्लिम पहचान को उजागर करने का है, न ही मैं गांधी पर कोई तथाकथित मजहबी प्रवचन या वाज करने की कोशिश करना चाहता हूं | इसके बरअक्स अल्लाह के नाम से अपनी बात शुरु करके मैं उस सवाल पर दोबारा लौटना चाहता हूं, जो आजकल जैसे ही खतरनाक राष्ट्रवादी माहौल में गांधी ने 1909 में पूछी थी | उनका सवाल था : क्या आधुनिक राष्ट्रवाद के नाम पर होने वाली राजनीति में दया-धर्म जैसे एहसास के लिए कोई स्थान है ? यकीनन यह गांधी का सवाल है; मेरा मानना है कि उनके लेखन में और उनके अमल में इस सवाल के अनेक बेहतरीन जवाब मिल सकते हैं | लेकिन यह सवाल इतनी सीधी तरह से हमारा सवाल नहीं बन सकता | अपनी पुस्तक ‘हिंद स्वराज’ में जिस बातचीत के जरिये गांधी इस सवाल तक पहुंचते हैं वैसी बातचीत न तो हम करते हैं और शायद करना भी नहीं चाहते हैं | तब बिस्मिल्लाह किस काम की ? मैं अपने ऐसे दो जाती तजुर्बे ब्यान करना चाहता हूं, जो शायद मेरे बिस्मिल्लाह पढ़ने के अमल को प्रासंगिक बना दें | मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूं और राजघाट से मेरा एक स्वाभाविक रिश्ता रहा है | बचपन की एक घटना है, शायद सातवीं या आठवीं क्लास की | ईद के अगले दिन अपने नए जूते पहन कर मैं स्कूल पहुंचा | नए जूते, ईद की खुमारी और क्रिकेट खेलने की लगन में बदहवास हम कुछ बच्चे राजघाट के सामने वाले पार्क में खेलने जा पहुंचे | खेल के बाद ठंडा पानी पीने की जरूरत हमें राजघाट के इलेक्ट्रिक पियाऊ तक ले गई | पानी पिया और सोचा कि चलो थोड़ा सुस्ता लिया जाए | हमने समाधि के चारों तरफ बने गलियारों में बैठने का फैसला किया | पर समस्या नए जूतों की थी ! समाधि के बाहर जूते रखना यानी उनके चोरी होने का खतरा | वैसे भी 1980 में राजघाट सिर्फ 2 अक्टूबर को ही जिंदा होता था | यह बात दूसरी है कि 1985 के बाद समाधियों की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन गई ! बहरहाल, हम जूते अंदर ले गए और एक गलियारे में जाकर बैठ गए | 10 मिनट भी न बीते थे कि तीन-चार चौकीदारों ने हमें आ दबोचा | उन्होंने पहले तो हमें दो-तीन थप्पड़ रसीद किए, फिर बताया कि हमारा गुनाह क्या था | यह अमल यहीं खत्म नहीं हुआ | हमें औपचारिक सजा दिलवाने के मकसद से कर्मठ गांधीवादी चौकीदार हमें समाधि के दफ्तर में मौजूद एक अधिकारी के पास ले गए | अधिकारी अहिंसावादी निकले | उन्होंने हमें थप्पड़ नहीं मारा | काफी प्यार से समझाया कि समाधि रसोईघर जैसी जगह है, जहां चप्पल-जूते ले जाना अच्छी बात नहीं है | हम इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हुए | हमने अपने नये जूतों की दुहाई देकर, जूते अंदर ले जाने की वजह बताने की कोशिश की | जिरह 5 मिनट भी न चली थी कि अहिंसक गांधीवादी अधिकारी विकराल सरकारी गांधीवादी में परिवर्तित हो गए और उन्होंने चिल्ला कर कहा - “ये ही नियम है | और आगे से ऐसा हुआ तो तुम्हें सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगा | दफा हो जाओ !” इस प्रसंग में वे अधिकारी और चौकीदार कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं | वे नियमबद्ध आधुनिक राज्य की नियमनप्रियता की प्रतीक हैं | दूसरी तरफ हम बच्चे, हमारे नए जूते और उनसे जुड़े एहसास! हम भी गलत नहीं हैं | तो फिर गलत क्या है ? मैं गांधी में इस गलत को तलाशना चाहता हूं | मेरा दूसरा तजुर्बा कुछ साल पहले का है | मैंने गांधी पर आयोजित एक कांफरेंस में परचा पढ़ा था | सेमिनार के बाद के एक मशहूर गांधी-विद्वान और कार्यकर्ता मुझसे स्वयं आकर मिले | मुझे नहीं मालूम कि उन्हें मेरा परचा पसंद आया था या मेरा मुसलमान नाम लेकिन उन्होंने मुझे बधाई दी और पूछा कि देश में मेरे जैसे कितने मुस्लिम विद्वान और कार्यकर्ता हैं, जो नयी गांधीवादी राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं ? प्रश्न अजीब था | मैं न तो कोई गांधी-विद्वान हूं और न ही कोई सियासी वोलंटीयर | मैंने कहा कि मेरी रूचि इस तरह के विषय पर सिर्फ शोध करने में है | वैसे भी आजादी के बाद मुसलमानों के बीच गांधी की पैठ पर कोई व्यवस्थित काम नहीं हुआ है | हमारे पास कुछ बेहद विरोधाभासी किस्से-कहानियां और यादें हैं, जिनके सहारे इस विषय पर बात होती रहती है | इस तर्क का समर्थन करते हुए इन विद्वान ने मुझसे ऐसे ही किसी किस्से के बारे बताने के लिए कहा | मैंने बताया कि मेरी नानी का परिवार बंटवारे के बाद दिल्ली में ही रह गया | जब भी हम नानी से सन 47 की बात सुनते हैं तो नानी नेहरु का नाम बेहद अदब और एहतराम से लेंती है | लेकिन जब भी गांधी पर बात होती तो वे या चुप हो जाती या फिर एक दर्द भरे गुस्से से कहती: उन्होंने मुसलमानों को मरवाया है !” दूसरी तरफ इससे बिलकुल उलटी भी तस्वीर है | मेरी पत्नी की एक वृद्ध महिला रिश्तेदार से बातचीत में हमें पता लगा कि बुलंदशहर के मुस्लिम बहुल गांवों में गांधी की मौत के 40 दिन बाद मुस्लिम रिवाजों से उनका चालीसवां हुआ था और इन चालीस दिनों तक लोगों ने मातम मनाया था | मेरा मत है कि गांधी से जुड़े इस तरह के विरोधाभासों पर काम हो | इतनी बात सुनकर उन गांधीवादी विद्वान के तास्सुरात बदल गए | वे मुझे समझाने लगे कि क्यों मेरी नानी गलत है और वे दूसरी महिला सही | धीरे-धीरे बातचीत में तल्खी आने लगी | वे गांधीवादी विद्वान गलत नहीं हैं | उनका उद्देश्य सही है | वे अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के प्रति ईमानदार हैं | वे नहीं चाहते कि इस माहौल में, जब कि गांधी का इस्तेमाल मुस्लिम-विरोध तक हो रहा है, इस तरह के उलझे हुए सवालों को सार्वजनिक किया जाए | लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं | मेरे शक-शुबहा जायज हैं | मैं बिना शोध किए यह नहीं मान सकता कि गांधी के प्रति लोगों का केवल एक नजरिया है - सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा, विश्वास है | एक शोधार्थी के नाते मेरा तो काम ही शक की बुनियाद पर टिका है | फिर गांधी का अपना तरीका भी रहा ही कि वे खुद, गीता सार में कहते हैं कि संदेह रहते विश्वास करना धर्म नहीं हो सकता है | विश्वास के लिए अनुभव और अनुभव के लिए प्रयोग हमें एक ऐसे सत्य से रू-ब-रू कराते हैं, जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसमें बदलाव की गुंजाइश होती है, और जो रोजमर्रा की व्यावहारिक जिंदगी की पेचीदगियों को अपने में समा लेने की क्षमता रखता है | शायद 1909 में गांधी आधुनिक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इसी दया-धर्म के सच की खोज का आह्वान कर रहे हैं | इसी तरह के प्रश्नों से उलझते हुए मुझे लगता है कि चंपारण सत्याग्रह से भारत छोड़ो आंदोलन तक की अलग रूपरेखा खींची जा सकती है | मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी रुचि ‘हिंद स्वराज’ में मौजूद पाठक नामक काल्पनिक पात्र में बिलकुल नहीं है | न ही मैं अपने को इस काबिल समझता हूं कि गांधी की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ संपादक बन जाऊं और एक नया ‘हिंद स्वराज’ लिख दूं | मैं ‘हिंद स्वराज’ की तर्क पद्धति में दिलचस्पी रखता हूं | बातचीत विमर्श बनाती है और विमर्श से ही तर्कों का निर्माण होता है | जरूरत है बातचीत और अनुभव से नैतिक निर्णय के निर्माण की | यहां मैं अकील बिलग्रामी का हवाला देना चाहूंगा | अपने एक लेख में वे कहते हैं कि गांधी को समझने के लिए नैतिक आलोचना और नैतिक निर्णय के बीच के अंतर को समझना जरूरी है | नैतिक आलोचना का अर्थ है किसी भी परिघटना या विचार की अपने तयशुदा नैतिक मूल्यों के आधार पर की जाने वाली आलोचना | लेकिन नैतिक निर्णय का मतलब है उस विचार को या घटना को अपने ऊपर लागू करना, उसे जीना और फिर एक तर्क या निर्णय पर पहुंचना | दूसरे शब्दों में कहें तो आलोचना को महज आलोचना तक सीमित करना विमर्श का अंत है जबकि आलोचना से निर्णय पर पहुंचना एक प्रक्रिया, जिसे गांधी बेहद सटीक शब्दों में ‘सत्याग्रह’ कह रहे हैं | गांधी कोई सत्याग्रही वैंगार्ड नहीं हैं जिसका काम क्रांति की अगुआई करना है बल्कि सत्याग्रही का मकसद अपने को अपने आप से बाहर लाना है, अपने विचारों को खोलना है और ऐसे नैतिक निर्णयों का निर्माण करना है, जो उसके स्वयं के जीवन को सामाजिक अर्थ दे सकें | सवाल पूछा जा सकता है कि क्या गांधी की इस पद्धति के हवाले से हम कहीं गांधीवाद और गांधीवादी राजनीति के कुछ मूल स्रोत खोजने की कोशिश तो नहीं कर रहे ? गांधी जैसे चिंतक को कुछ स्रोत-बिंदुओं तक सीमित करना बेहद खतरनाक काम है | वह भी तब जब कि वे स्वयं इस तरह के वैचारिक अमल का खुला विरोध करते नजर आते हैं | 1945 में नेहरु को लिखे एक खत में गांधी कहते हैं: “मैंने कहा है कि ‘हिंद स्वराज’ में मैंने जो लिखा है उस राज्यपद्धति पर मैं बिलकुल कायम हूं | यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, लेकिन जो चीज मैंने सन् 1909 में लिखी है उसी चीज का सत्य मैंने अनुभव से आज तक पाया है | आखिर मैं उसे मानने वाला एक ही रह जाऊं, उसका मुझको जरा-सा भी दुख न होगा क्योंकि मैं सत्य जैसा पाता हूं उसका ही साक्षी बन सकता हूं | ‘हिंद स्वराज’ मेरे सामने नहीं है | अच्छा है कि मैं उसी चित्र को आज अपनी भाषा में खींचूं | पीछे वह चित्र सन् 1909 जैसा ही है या नहीं, उसकी मुझे दरकार न रहेगी, न तुम्हें रहनी चाहिए | आखिर मैंने पहले क्या कहा था, उसे सिद्ध करना नहीं है | आज मैं क्या कहता हूं, वही जानना आवश्यक है |” ‘हिंद स्वराज’ ऐसी किताब है जिसमें गांधी ने कभी कोई तरमीम करने की जरूरत नहीं समझी | उनका कहना था कि यदि एक ही विषय पर उनके दो विरोधाभासी लेखन मिलें तब उनकी उसी राय को सही माना जाए, जो समय-क्रम में बाद के किसी लेख में लिखी गई हो | लेकिन इस खत में वे एक कदम आगे जाकर ‘हिंद स्वराज’ पर भी एक सवाल उठाते देखे जा सकते हैं | ‘हिंद स्वराज’ उनके लिए एक रूपरेखा है, जिसके जरिए एक अलग तरीके का चित्र खींचना मुमकिन भी है और जरूरी भी | इस खत की दूसरी अहम बात है नैतिक निर्णय का खुलापन | गांधी कहते हैं कि ‘हिंद स्वराज’ की प्रासंगिकता उनके अनुभव से ताल्लुक रखती है | इसलिए वे इसकी रूपरेखा को सही मान रहे हैं | लेकिन ‘हिंद स्वराज’ की स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं हैं कि इस किताब में कोई राजनीतिक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, बल्कि यहां एक अनुभवनिष्ठ प्रक्रिया का जिक्र है जिसका अपना एक नैतिक मूल्य है | तभी तो गांधी कहते हैं: आधुनिक शास्त्र की कदर करते हुए पुरानी बातों को मैं आधुनिक शास्त्र की निगाह से देखता हूं तो पुरानी बात नये लिबास में मुझे बहुत मीठी लगती है |” दूसरा उदाहरण गांधी के राजनीतिक अमल की अप्रत्याशित प्रवृत्ति से है | गांधी पर अकसर आरोप लगाया जाता है कि उनके आंदोलन अप्रत्याशित होते थे, जो न सिर्फ सरकार को बल्कि उनके अपने साथियों को भी हैरान कर दिया करते थे | अपने दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों और प्रयोगों का जिक्र करते हुए गांधी एक स्थान पर लिखते हैं: सत्याग्रह की खूबी यह है कि यह मनुष्य तक स्वयं आता है, यह सद्गुण सत्याग्रह के सिद्धांत में अंतनिर्हित है | धर्मयुद्ध में किसी भी पक्ष को छिपाने की जरूरत नहीं होती, असत्य नहीं होता, मक्कारी नहीं होती | पहले से तयशुदा रणनीति के आधार पर किया गया संघर्ष हकपरस्त तहरीक नहीं हो सकता | सच्चे संघर्ष में ईश्वर स्वयं अभियान की नीति निर्धारित करता है और स्वयं ही धर्मयुद्ध का संचालन करता है | इससे साफ है कि गांधी के संघर्ष, उनकी राजनीति और उनके दया धर्म का सार उनके अपने संदर्भ में लिप्त है | वे अपने उस आज का अहम हिस्सा है, जिसे हम 1917 से 1948 तक का इतिहास कहकर छुट्टी पा लेते हैं | अगर गांधीवाद की खोज गांधी को हमसे दूर ले जाती है, अगर गांधी के अनुभव हमें सिर्फ उन संदर्भलिप्त नैतिक की तरफ ले जाते हैं जो अपने आप में बेहद महीन और लचीले हैं, तब वह क्या संभव तरीका हो सकता है जिसके जरिये गांधी हमारे समकालीन बन सकते हैं ? गांधी को अपना समकालीन बनाने की कवायद करने के लिए हम चार संभव प्रयास कर सकते हैं -
मेरे अंदर का पेशेवर शोधार्थी पहले तीन चरणों तक जाने में कोई झिझक महसूस नहीं करता है पर इस प्रयास का चौथा कदम थोड़ा पेचीदा है | मैं इस पक्ष पर बाद में लौटूंगा, फिलहाल बात की जाए हमारे युग के मूल प्रश्नों की | मूल प्रश्नों का चुनाव इतना आसान काम नहीं है | एक व्यक्ति या समूह के लिए जो मुद्दा मूल प्रश्न हो सकता है, वही किसी दूसरे समुदाय के लिए बिलकुल बेबुनियाद हो सकता है | यह भी कहा जा सकता है कि मूल प्रश्न का पूरा विचार ही गलत है | गांधी अपने लेखन में इस बात को बेहद महत्त्व देते दिखते हैं | उनके दो मुख्य पुस्तकें ‘हिंद स्वराज’ और ‘रचनात्मक कार्यक्रम’ इस मामले में उल्लेखनीय हैं | इन किताबों में विषयों का चुनाव और उनका क्रम बेहद दिलचस्प है | गांधी बार-बार याद दिलाते हैं कि क्यों कोई बात पहले की जा रही है और क्यों किसी बात को केहने के लिए भूमिका बांधने की जरुरत है | गांधी यह भी कहते हैं कि जिन सवालों को वे मूल प्रश्न कह रहे हैं उनका चुनाव गांधी का अपना है और वे इन सवालों को किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय पर थोपने के पक्षधर नहीं हैं | गांधी की आत्मकथा की भूमिका में यह खुलासा बेहद साफ मिलता है | गांधी को समकालीन बनाने के प्रयास की दूसरी शर्त यह है कि वैसा ही कोई सवाल या उससे मिलता-जुलता मुद्दा हम लें, जो गांधी के लिए भी मूल प्रश्न रहा हो | यह शर्त मूल प्रश्न की हमारी तलाश को थोड़ा आसान और व्यवस्थित कर देती है | हमारे पास हमारा आज भी है और गांधी का आज भी | हमारे आज के बिखराव की अपनी विशिष्टता है, जिसे हम वर्तमान कहकर एक परिधि में बांधने की कोशिश करते हैं | इसके बरअक्स गांधी का आज एक व्यवस्थित इतिहास बन चुका है, जिसमें एक शुरुआत है और एक अंत भी है | सरकारी नारा ‘संकल्प से सिद्धि,’ जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े उत्साह से प्रतिपादित किया है, इसी इतिहास-बोध का उदाहरन है | इसे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो 1942 में ही तय हो चुका था कि 1947 में क्या होगा ! गांधी अपने आज को इतिहास की इस स्थूल और बासी समझ से परे रखते हैं | वे ‘हिंद स्वराज’ में कहते हैं: “हिस्टरी अस्वाभाविक बातों को दर्ज करती हैं | सत्याग्रह स्वाभाविक है, इसलिए उसे दर्ज करने की जरूरत ही नहीं है |” (हिंद स्वराज, 1949, पृ. 63) इतिहास-मुक्त गांधी और हमारे आज के विमर्श का सम्मिलन कुछ ऐसे मुद्दों की ओर इशारा करता है, जो उलझे हुए भी हैं और जिन पर बातचीत भी नहीं होती है | ये सवाल हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं और सत्याग्रह की राजनीति के अंतर्संबंधो के | क्या चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक आम भारतवासी की भागीदारी का अर्थ सिर्फ और सिर्फ वोट डालना है ? लोकतंत्र में विरोध की राजनीति के लिए कितनी गुंजाइश है ? क्या चुनी हुई सरकार का विरोध करना लोकतंत्र का विरोध है ? क्या इस लोकतंत्र में उस दया-धर्म के लिए कोई जगह है जिसकी चर्चा गांधी ‘हिंद स्वराज’ में करते हैं ? ये प्रश्न मेरी अपनी आज की समझ और गांधी के लेखन की मेरी निजी व्याख्या से निकले हैं इसलिए मैं भी गांधी की तरह अनुरोध करता हूं कि इस सवालों को आरोपित सत्य के रूप में न देखा जाए | मुझे लगता है कि हम इस बहस में न पड़ें कि ये मूल प्रश्न हैं या नहीं, बल्कि इस बात को टटोला जाए कि इन सवालों के जवाब तलाशने का व्यापक तरीका क्या हो ? मेरा मत है कि इसकी शुरुआत हमारी आज की स्वीक्रत राजनीतिक नैतिकता से करना जरूरी है | भारतीय लोकतंत्र और उसमें विरोध की राजनीति को समझने के लिए हमें भारतीय संविधान को अलग नजरिए से देखना होगा | मेरा मत है कि संविधान के विचार, उसके मूल्य और उसमें मौजूद शक्तियों के बंटवारे के बीच के फर्क और अंतर्संबंधो को रेखांकित करना बेहद जरूरी है | हमारा संविधान कुछ बुनियादी मानवीय विचारों पर आधारित है | ये विचार-मूल्य स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, सामाजिक बराबरी और मजहबी आजादी सिद्धांत के रूप में काम करते हैं ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए जा सकें | शक्तियों के इसी बंटवारे के आधार पर सरकार बनती है, कानून बनते हैं और उनको लागू करने के प्रावधानों का विवेचन होता है; यानी सरकार और कानून उन मूल्यों को अमली जामा पहनाते हैं जो मानवीय हैं, न कि सरकारी | निस्संदेह भारतीय संविधान एक उम्दा दस्तावेज है, जो हमारी राज्य-व्यवस्था को एक कानूनी परिधि में बांधता है | लेकिन संविधान कोई पवित्र किताब नहीं हो सकता | यह एक मानव-निर्मित दस्तावेज है, जो एक खास राजनीतिक संदर्भ में अस्तित्व में आया | इसकी सफलता का मूल कारण इसका लचीलापन है | वास्तव में संविधान में संशोधन और परिवर्तन करने की गुंजाइश ने ही इसे एक जिंदा दस्तावेज में परिवर्तित कर दिया है | संविधान की सफलता का एक पक्ष और भी है | संविधान आज की भारतीय राजनीति का मूल वैचारिक स्रोत है | संविधान के नाम पर ही राजनीतिक दलों की विचारधाराओं का निर्माण और पुननिर्माण होता है, संविधान के नाम पर ही किसी भी राजनीतिक अमल को सही या गलत ठहराया जाता है, संविधान के नाम पर ही शासन होता है और दिलचस्प तो यह है कि संविधान के नाम पर ही शासन का राजनीतिक विरोध भी होता है | कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति के घालमेल में संविधान एक मुहावरा है, जिसके जरिये राजनीति की स्वीक्रत जबान का निर्माण होता रहा है | संविधान के इस महिमागान के बीच राजनीतिक नैतिकता का सवाल अहम है | अगर हमें किसी राजनीतिक मुद्दे पर अपनी असहमति जतानी हो तो क्या वह जरूरी है कि पहले हम संविधान की कसम खाएं, फिर भारत की प्रभुसत्ता की रक्षा का दवा करें, फिर संविधान के किसी अनुच्छेद की दुहाई दें और फिर भी काम न बने तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दें ? मेरा मत है कि संविधान के मूल्यों की रक्षा का अर्थ राज्य संस्थाओं की संरचनाओं और उनके व्यवहारों की अंध-भक्ति नहीं है | यहीं आकर गांधी बेहद प्रासंगिक हो जाते हैं | वे अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस तरह के सवालों से उलझते रहे | उनका राजनीतिक विमर्श सत्ता के साथ सत्याग्रही संबंध और स्वराज की आजाद समझ की परिधि के बीच निर्मित होता है | 1921 में वायसराय ने जब कहा था कि भारत में स्वराज तलवार के बल आ सकता है या फिर ब्रिटिश संसद की दरियादिली की वजह से, तब गांधी ने लिखा था : “वायसराय के इस विचार से मेरा पूर्णत: मतभेद है कि यदि स्वराज तलवार की शक्ति से नहीं आता तो वह अवश्य ही ब्रिटिश संसद की ओर से आएगा | जब लोगों की इच्छा की ‘तलवार’ अदम्य हो जाएगी तब ब्रिटिश संसद उसकी पुष्टि करेगी | असहयोगी इस्पात की तलवार के बदले आत्मोत्सर्ग की तलवार को प्रयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं, यह जानने के लिए हमें अधिक काल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी |” गांधी के विचार में ब्रिटिश संसद का काम स्वराज की जन-भावना को मंजूरी देना भर है ताकि परिवर्तन की संस्थागत गतिशीलता बनी रहे | यहां यह बताना जरूरी है कि स्वराज की जन-भावना का अर्थ बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा नहीं है | गांधी ‘हिंद स्वराज’ में साफ कहते हैं कि स्वराज का अर्थ नंबर गेम नहीं है | उनका मत है कि सिर्फ इसलिए कि भारत में हिंदुस्तानी ज्यादा हैं और अंग्रेज कम, भारत में स्वराज आना चाहिए, गलत धारणा है | स्वराज का अर्थ है सत्य और अहिंसा के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण और राजनीति में मूलभूत परिवर्तन | स्वराज की इस रूपरेखा में स्थानीय निकायों (जैसे नगरपालिका) से लेकर ब्रिटिश संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपना विशिष्ट स्थान है | गांधी इन संस्थाओं को उनके जन-प्रतिनिधित्व करने के दावे की वजह से स्वीकारते हैं | लेकिन इन संस्थाओं में निहित विधायी और कार्यकारी शक्तियां उनके लिए कोई खास नैतिक मूल्य नहीं रखतीं | यही कारण है कि गांधी खुद को व्यावहारिक आदर्शवादी बताते हैं : “मैं खुद को व्यावहारिक आदर्शवादी मानता हूं | मेरा निजी मत है कि विधायिका स्वराज लाने का जरिया नहीं हो सकती |” “मैं खुद को एक व्यावहारिक आदर्शवादी मानता हूं | मैं जनता के संदर्भ में स्वराज प्राप्त करने के साधन के रूप में विधानसभाओं में अपना अविश्वास बरकरार रखूंगा |” (ए.आइ.सी.सी. में भाषण, पटना- 1 मई 1934) गांधी द्वारा विधायिका में अविश्वास व्यक्त करने के अर्थ यह नहीं है कि वे लोकतंत्र के समर्थक नहीं हैं | 1928 में जब देश में ब्रिटिश विरोध अपने चरम पर था, गांधी ने ‘यंग इंडिया’ में लिखा था: “अगर हम लोकतंत्र की भावना को विकसित करना चाहते हैं तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारा दृष्टिकोण अपने मुखालिफ के प्रति कैसा हो | हमें सरकार की गुलामी खत्म करके असहयोगियों और सरकार के मुखालिफों की नई गुलामी कायम नहीं करनी है | हम अपने मुखालिफ के लिए भी वही आजादी चुनें, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं |” गांधी का संघर्ष लोकतंत्र की भावना के लिए है, वे उस राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सेवाभाव और दयाधर्म हो | यही कारण है कि 1937 के अपने एक अन्य भाषण में गांधी संस्थाओं के संविधान, उनके नियम उपनियम और उनको चलाने वालों के व्यवहारों के फर्क को उजागर करते हैं | गांधी की ये बातें कोरी लफ्फाजी नहीं हैं न ही एक लाचार बूढ़े की सलाह | 1946 तक आते-आते यह लगभग तय हो गया था कि भविष्य का भारत ब्रिटिश संसदीय मॉडल को अपनाएगा | इस परिप्रेक्ष्य में गांधी इस बात को भांप रहे थे कि भविष्य की संसद एक पेशेवर राजनीतिक संस्था बन सकती है और भविष्य के चुने हुए प्रतिनिधि पेशेवर नेता | इस खतरे से निबटने के लिए गांधी एक व्यावहारिक सलाह देते हैं : “विधायक सरकार की नीतियों को पारदर्शी बनाने का काम कर सकते हैं | यह उनकी सबसे बुनियादी सेवा होगी पर उनका प्रमुख कर्तव्य तो यह है कि वे आमलोगों को बताएं कि सरकार की कमियों को जानने के बावजूद वे क्यों और कैसे सरकारी नीतियों के शिकार हो जाते हैं, वे जनता को जागरूक करें और उसे सरकार की अन्यायपूर्ण और गलत नीतियों के खिलाफ खड़े होने के लिए शिक्षित करें | विधायकों का दूसरा काम जन-विरोधी कानूनों को बनने से रोकना है और ऐसे कानून बनाने का मार्ग खोलना है जो तामीरी काम में मददगार हो |” गांधी के इस कथन से साफ जाहिर है वे प्रतिनिधित्व के सवाल को महज कानून बनाने तक सीमित करके नहीं देखते | उनके लिए विधायकों का काम जन चेतना की नुमाइंदगी करना है | यहां तक कि अगर कोई चुनी हुई सरकार जन विरोधी काम करे तो वे जनता को सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करें | सवाल पूछा जा सकता है ऐसे विधायकों की खोज करने के बजाय गांधी ने स्वयं संविधान-निर्माण में हिस्सा क्यों नहीं लिया ? वे क्यों नहीं सरकार में शामिल होकर सरकार चालाने लगे ? दिसंबर 1947 में हिंदुस्तानी तालीम संघ की एक बैठक में डॉ. जाकिर हुसैन ने गांधी से यही सवाल पुछा था : “डॉ. जाकिर हुसैन: विभिन्न संस्थाएं कुछ विशेष कार्य करने के लिए तदर्थ समितियों के रूप में अलग-अलग बनाई गई थीं | यदि अब उन्हें मिलाकर एक संस्था बना दिया गया तो उस संस्था को सत्ता की राजनीति से दूर रखना असंभव होगा ?” “गांधीजी: यदि संयुक्त रचनात्मक कार्यकर्ता संघ सत्ता की राजनीति में पड़ने की कोशिश करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा | अन्यथा क्या मैं स्वयं सत्ता की राजनीति में घुसकर सरकार को अपने तरीके से चलाने का प्रयाक न करता ? आज जो सत्ता की बागडोर संभाले हैं, वे आसानी से अलग हो जाते और मुझे अपनी जगह दे देते लेकिन जब तक सत्ता उनके अधिकार में है, वे अपने ही विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं | मगर मैं सत्ता अपने हाथ में लेना नहीं चाहता | हम सत्ता से परे रहकर और मतदाताओं की शुद्ध नि:स्वार्थ सेवा करके उनका मार्गदर्शन करते हुए उन पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं | ऐसा करके हम उससे कहीं अधिक सच्ची सत्ता प्राप्त कर सकेंगे, जो हमें सरकार में शामिल होने पर प्राप्त होगी | मगर एक वक्त ऐसा आ सकता है जब लोग यह महसूस करें और कहें कि वे चाहते हैं कि कोई और नहीं बल्कि हम ही सत्ता संभालें | तब इस सवाल पर विचार किया जा सकेगा | बहुत संभव है कि मैं तब तक जीवित ही न रहूं | लेकिन जब ऐसा समय आएगा तब संघों में से कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा जो शासन की बागडोर संभालेगा | उस समय तक भारत एक आदर्श राज्य बन जाएगा | “डॉ. जाकिर हुसैन : काय हमें एक आदर्श राज्य का शुभारंभ करने और उसे चलाने के लिए आदर्श पुरुषों की आवश्यकता नहीं होगी ?” “गांधीजी : हम स्वयं सरकार में शामिल हुए बिना भी अपनी पसंद के लोगों को सरकार में भेज सकते हैं | आज कांग्रेस में हर आदमी सत्ता के पीछे भाग रहा है | यह बहुत बड़े खतरे का संकेत है | हमें सत्ता-लुप्सुओं की भागदौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए |” गांधी की इस समझ में मतदाता संसदीय लोकतंत्र नामक मशीन का पुर्जा नहीं है | उनके लिए वोटर सत्याग्रही है | इस सत्याग्रही को संगठित करने के लिए वे संसद के बाहर रहकर जन-संस्थाओं के निर्माण का आह्वान करते हैं ताकि लोकतंत्र की सच्ची भावना की कवायद जारी रहे | यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि गांधी का सत्याग्रही वोटर न तो नेहरुवादी कांग्रेस का वह आम आदमी है, जिसे मॉडर्न बनाना लाजिमी है और न ही ‘टाटा टी’ के विज्ञापन में आने वाला जागरूक मतदाता | उनके लिए राजनीतिक अधिकारों की पहचान एक प्रक्रिया है, जिसके जरिये दया-धर्म पर आधारित व्यापक स्वतंत्रता को आम जिंदगी में हासिल किया जा सकता है | वोटर और उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के इसी रिश्ते को गांधी 1937 के अपने एक भाषण में बेहद सटीक तरीके से बताते हैं | 1935 के अधिनियम के विशेष संदर्भ में दी गई इस तकरीर में वे कहते हैं: “अब इस पर एक और दृष्टी से विचार कीजिए | विधान-मंडलों में लोग एक निश्चित, सीमित संख्या में ही सदस्य बनकर जा सकते हैं, शयद पंद्रह सौ ही सदस्य बन सकते हैं | यहां उपस्थित लोगों में से कितने लोग उनके सदस्य बन सकते हैं ? और फिलहाल इन पंद्रह सौ सदस्यों के लिए मतदान करने का अधिकार केवल साढ़े तीन करोड़ लोगों को ही प्राप्त है | शेष साढ़े इकतीस करोड़ से अधिक लोगों का क्या होगा ? स्वराज की हमारी संकल्पना के अनुसार तो ये साढ़े इकतीस करोड़ ही देश के साचे मालिक हैं और ये साढ़े तीन करोड़ मतदाता, जो पंद्रह सौ विधायकों का भाग्य करेंगे, उसके सेवक ही हैं | इस प्रकार पंद्रह सौ विधायक यदि अपने विश्वास के प्रति सच्चे रहें तो वास्तव में ये समूची जनता के दोहरे सेवक होंगे | लेकिन साढ़े इकतीस करोड़ लोगों को स्वयं अपने प्रति, और व्यक्तियों के रूप में वे जिसके अंश हैं उस राष्ट्र के प्रति भी, अपने दायित्व का निर्वाह करना है | यदि वे स्वयं काहिल बने रहे और उन्होंने यह जानने-समझने की कोशिश नहीं की कि स्वराज्य क्या है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है, तो वे पंद्रह सौ विधायकों के गुलाम बनकर रह जाएंगे | इस हिसाब से साढ़े तीन करोड़ मतदाता भी साढ़े इकतीस करोड़ आम जनता की श्रेणी में ही आते हैं | इसलिए कि यदि वे मेहनती और जागरूक न बने, तो वे भी पंद्रह सौ खिलाड़ियों के हाथ में, आम जनता की भांति, खिलौने-भर बनकर रहे जाएंगे | फिर वे खिलाड़ी कांग्रेसी विधायक हों या अन्य किसी दल के, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता | यदि मतदाता हर तीन साल या ऐसी ही किसी अवधि के बाद केवल अपना मतदान करने के लिए ही आंखें खोलें और उसके बाद फिर से सो जाएं, तो उनके सेवक ही उनके मालिक बन बैठेंगे | “ऐसी विपत्ति से बचने का एक ही उपाय मैं जानता हूं - कि सभी पैंतीस करोड़ लोग मेहनती और समझदार बनें | ऐसा तभी हो सकेगा जब वे चरखे और अन्य ग्रामोधोगों को अपना लें | वे इनको बिना समझे-बूझे न अपनाएं | मैं अपने अनुभव से आपको बतला सकता हूं कि ऐसा प्रयत्न करने का अर्थ है - सही किस्म की वयस्क शिक्षा देना और इसके लिए जरूरी है धैर्य, नैतिक मनोबल और अपनी पसंद के जिस भी गांव में, आप जो भी धंधा शुरु करना चाहते हों उसकी वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक जानकारी हासिल करना |” मैंने पहले कहा है कि गांधी के विचारों से सूत्र विचार निकालना गांधी की अपनी पद्धति के विरुद्ध जाता है | इसलिए अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं और सत्याग्रही आंदोलन से संबंधित गांधी के विचारों को, जिनकी चर्चा हमने यहां की है, समेटें तो एक चारपक्षीय वक्तव्य अभिव्यक्त किया जा सकता है :
यहां मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी के सवाल और हमारे सवाल अलग हैं | गांधी के जवाब उनके अपने आज को मुखातिब करते हैं जबकि हमें अपने आज को अलग तरीके से संबोधित करना होगा | गांधी से जो हम ले सकते हैं वह है उनकी प्रयोगधर्मिता; और यही गांधी को समकालीन बनाने के प्रयास का तीसरा कदम है | गांधी की पद्धति से देखें तो साफ है कि विरोध की राजनीति के मूल मैं लोकतांत्रिक भावना छिपी हुई है | भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित दावे इसी भावना को चरितार्थ करते हैं | इसलिए जन-विरोधी नीतियों का विरोध लोकतांत्रिक भी है, तर्कसम्मत भी है, और संवैधानिक भी | लोकतांत्रिक विरोध को राष्ट्रद्रोह कहना संविधान की आत्मा और सत्याग्रह के विचार का अपमान है | चुनाव जीत कर आए हमारे प्रतिनिधि भूल जाते हैं कि उनका काम पार्टी-पूजा और नेता-पूजा नहीं है | जब वे संविधान की शपथ लेते हैं तो वह संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को अपनाने की शपथ होती है, न कि राज्यसत्ता भोगने का पांच साल का कांट्रैक्ट, क्योंकि संसद का काम जन-विरोध का संस्थागत विरोध करना है | विरोध करने के इस रैडिकल आह्वान का एक दूसरा पहलू भी है, जो विरोध की नैतिकता से ताल्लुक रखता है | विपक्ष में मौजूद दल संविधान का इस्तेमाल विरोध करने के लिए करते ही हैं | लेकिन यह पेशेवर विरोध, सत्ता सुख के लिए होता है, न कि जन भावना को अभिव्यक्त करने के लिए | संसद में विपक्ष द्वारा नोटबंदी और जीएसटी पर जताए गए पेशेवर विरोध के बावजूद अगर देश में पनप रही आर्थिक मंदी राजनीतिक सवाल नहीं बन पाती है तो साफ है कि विपक्ष का विरोध जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है | गांधी के चश्मे से देखें तो (शर्त यह है कि चश्मा ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के विज्ञापन में दिखने वाला नहीं होना चाहिए !) यह कहा जा सकता है कि विरोध करने के लिए विरोध करना, व्यक्ति या समुदाय की कुछ मांगो को मनवाने के लिए विरोध करना, और सत्ता-प्राप्ति के लिए विरोध करना सत्याग्रही विरोध नहीं हो सकता | सयाग्रही विरोध दूसरों को ज्ञान बांटने, राजनीतिक रोडमैप बनाने और देने, ‘संकल्प से सिद्धि’ जैसे नारों और राजनीतिक जुमलेबाजी का नाम नहीं है | यही बात लोकतंत्र की आज की समझ से भी जुड़ती है | लोकतंत्र का अर्थ चुनाव बाजार नहीं है, जिसमें राजनीतिक दल अपने ब्रांड और अपने चुनावी वायदे लेकर वोटर को उपभोक्ता की तरह लुभाते हैं, न ही चुनाव जीतने की क्षमता, जिसे आजकल ‘विनेबिलिटी’ कहा जाता है, जनमत होती है | तो फिर सत्याग्रही विरोध का आज का मुहावरा क्या हो सकता है ? यही गांधी की समकालीनता को पाने का चौथा कदम है जिसकी ओर हमने शुरुआत में इशारा भर किया था | इस सवाल का जावाब देना किसी एक व्यक्ति या संस्था का काम नहीं है | गांधी की मानें तो इस सवाल का जवाब इतिहास में तलाशना निरर्थक होगा | वैचारिक चक्रव्यूह से निकलने के लिए ‘क्या है’ और ‘क्या होना चाहिए’ के बीच फर्क करना जरूरी है | हम सभी यह बताने में तत्पर रहे हैं कि क्या होना चाहिए लेकिन जिस आज में हम रहते हैं उसकी पेचीदगियों को जानने-समझने की लिए हम तैयार नहीं हैं | हमें लगता है कि आज से हम पूरी तरह बा-खबर हैं और मसला सिर्फ भविष्य का है | गांधी इस तथ्य के सख्त मुखालिफ थे | इसीलिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आज को सामूहिक प्रयास से जानना चाहिए | शायद तब मुमकिन है कि दया-धर्म के कुछ नए मायने सामने आएं | शायद तब बिस्मिल्लाह पढ़कर बात शुरु करने और गीता के श्लोक से बात खत्म करने के बावजूद महंगाई, भूखमरी और जन अधिकारों की रौडिकल चर्चा की जा सके | यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत; अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् | सौजन्य : 'गांधी मार्ग', नवंबर-दिसंबर २०१७ (गांधी शांति प्रतिष्ठान की वार्षिक व्याख्यानमाला में 2 अक्तूबर 2017 को दिया व्याख्यान | देशी-विदेशी संस्थाओं में अध्ययन कर चुके हीलाल अहमद राजनीति तथा इतिहास के अध्येता व शोधकर्मी हैं और अल्पसंख्यक समाज के साथ गांधी के संदर्भ को जोड़ने का काम गहरी आस्था व प्रखरता से करते हैं |) |